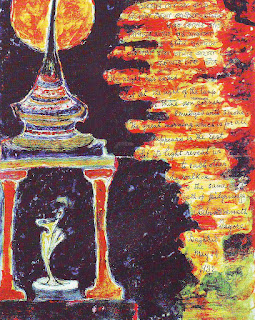कल आनंदकुमार स्वामी को पढ़ रहा था। वह स्थापित करते हैं, ‘नवीनता नवीन बनाने में नहीं, नवीन होने में है।’ इस समय जब भारतीय शास्त्रीय कलाओ पर विचारता हूं तो उनका यह कहा गहरे से घर करता है। शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला का मूल वही है, शास्त्रीय गायन,वादन में मूल राग वही है जो बरसों से हम सुनते आए हैं फिर भी इन शास्त्रीयकलाओं में कलाकार सदा प्रस्तुति में नवीन करता है। इस नवीन में ही रसानुभूति हैं। फिर से कुछ सुनने, फिर से कुछ गुनने की। परन्तु अपसंस्कृति के इस समय में शास्त्रीय कलाओं का यह मूल हमसे जैसे निरंतर दूर भी हो रहा है।
बहरहाल, भारतीय दर्षन में कलाओं को शुद्ध रूप से जीवन से अभिहित किया गया है। ऐसा जब है तो फिर क्या यह विचारणीय नहीं है कि हम अपनी शास्त्रीय कलाओ के नवीनता के उस मूल को कितना बचाए रख पा रहे हैं? मुझे लगता है, कुछेक लोकप्रिय कलाओं को छोड़ हम बहुतेरी हमारी सांस्कृतिक कलाओं से लगातार दूर और दूर हुए जा रहे हैं। कभी राजस्थान के मांगणियारों, लंगो का लोक संगीत धोरों की अनूठी रेत राग से मेल कराता कानों में शहद घोलता था, उसे नवीन बनाने के चक्कर में सूफी संगीत लोक संगीत बन गया है। इसी तरह शास्त्रीय संगीत के स्वर भी बहुत से स्तरों पर फ्यूजन में कनफ्यूज हो रहे हैं। शास्त्रीय नृत्यों को कोरियोग्राफी के नाम बिगाड़ शारीरिक लयकारी में तब्दील किया जा रहा है। चित्रकला में इन्स्टालेषन के नाम पर मनमानी हो ही रही है। सोचता हूं, ऐसा ही होता रहा तो आने वाली पीढ़ी में कलाओं का हमारा मूल क्या कुछ बचा भी रहेगा!
कुछ समय पहले अषोक वाजपेयी के नेतृत्व में पं. बिरजू महाराज, पं. हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन, पं. राजन-साजन मिश्र, पं. षिवकुमार शर्मा, टी.एन. कृष्णन, सुधा रघुनाथन, यू.श्रीनिवासन आदि कलाकारो के एक दल ने मिलकर षास्त्रीय कलाओं के संरक्षण के लिये संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इसके तहत शास्त्रीय कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिये बड़े व्यावसायिक घरानों की एक प्रतिषत आय को आयकर मुक्त कर उसे सांस्कृतिक गतिविधियों मंे लगाने, अलग से सांस्कृतिक टेलीविजन चैनल स्थापित करने आदि की मांग की गयी थी। इन मांगों पर सरकार ने क्या किया है और क्या कुछ करने जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता परन्तु सोचने की बात यह भी है कि शास्त्रीय कलाओ के लिये खुद समाज क्या कर रहा है? स्पीक मैके, श्रुति मंडल और सरकारी संस्थाएं, अकादमियां अपने स्थायी आयोजनों में कलाओं का प्रदर्षन, प्रोत्साहन के उपक्रम करती भी हैं परन्तु शास्त्रीय कलाओं के आयोजन से ही क्या हम हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मूल रूप में सहेज पाएंगे? शास्त्रीय कलाओं के अपसंस्कृतिकरण, अरूपीकरण को क्या इससे रोका जा सकता है? इन पर गहरे से विचारने की जरूरत है।
यह सही है कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं के आयोजनों से इन कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है परन्तु इतना ही सच यह भी है कि इनसे नया कोई श्रोता वर्ग, दर्षक वर्ग खड़ा नहीं किया जा रहा। वही है जिनकी रूचि शास्त्रीय कलाओं में है। फिर से गौर करें, रसिकता नया बनाने से नहीं नये होने से ही पैदा की जा सकती है। इसका अर्थ है, आयोजनों के पार्ष्व में भी इस ‘नये होने’ पर विचार करना होगा। सोचता हूं, अभिनेता आमीर खान ने ‘सत्यमेव जयते’ में वही कुछ कहा है, उसी पर ध्यान दिलाया है जिस पर अरसे से कहा, ध्यान दिलाया जाता रहा है परन्तु प्रस्तुति के और मंषा के उनके नयेपन से उनके शो ने अधिसंख्य लोगों का ध्यान खींचा है। शास्त्रीय कलाओं की प्रस्तुतियों के साथ कलाओं की सहज समझ, जानकारियां, रसिकता के लिये भी कुछ ऐसा ही नया करना होगा।
उस्ताद अमीर खॉं, पं. भीमसेन जोषी, पं. जसराज ने वही राग गाए हैं जो उनसे पहले गायक गाते आए हैं, पं. बिरजू महाराज ने वह नृत्य किया जो पहले होता रहा परन्तु इन सबने अपने को मूल में साधा। पुनर्नवा किया। आनंद कुमार स्वामी इसीलिये फिर से याद आ रहे हैं, ‘नवीनता नवीन बनाने में नहीं नवीन होने में है।’ शास्त्रीय कलाओं को बचाने, उनके संरक्षण के लिये यही मूल मंत्र हो सकता है।
.jpg)